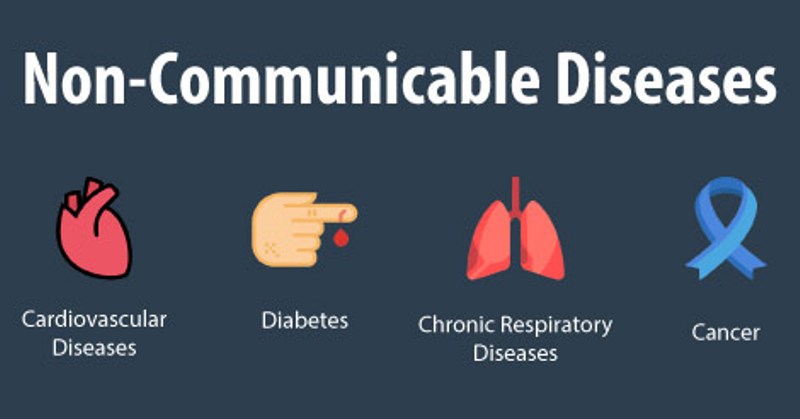Daily Current Affairs 4 July 2019
Daily current affairs:-We have Provided Daily Current Affairs for UPSC and State PCS Examinations. Current affairs is the most Important Section in the UPSC examination. To get more score in the current affairs section must Visit our Website Daily Basis.
यूजीसी ने भारत में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल ‘स्ट्राइड’ को मंजूरी दी
भारत में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एक नई पहल ‘स्कीम फॉर ट्रांस-डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकॉनमी (स्ट्राइड) को मंजूरी दी।
प्रमुख बिंदु:
महत्व: यह सहयोगी अनुसंधान के साथ भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था की दिशा में योगदान करने के लिए छात्रों और शिक्षकों की सहायता करके कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान संस्कृति और नवाचार को मजबूत करेगा।
पहल: योजना के तहत महत्वपूर्ण पहल ‘रिसर्च प्रोजेक्ट’, ‘रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग’ और ‘इनोवेशन’ हैं।
उद्देश्य: इसका उद्देश्य युवा प्रतिभाओं की पहचान करना, अनुसंधान संस्कृति को मजबूत करना, क्षमता का निर्माण करना, नवाचार को बढ़ावा देना, ट्रांस-डिसिप्लिनरी रिसर्च का समर्थन करना और मानविकी और मानव विज्ञान में बहु-संस्थागत नेटवर्क उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान परियोजनाओं को निधि (फण्ड) प्रदान करना है।
घटक: योजना के 3 घटक हैं। घटक 1- प्रेरित युवा प्रतिभाओं की पहचान करना (1 करोड़ तक के अनुदान के लिए सभी विषयों के लिए लागू) , घटक 2- समस्या को सुलझाने के कौशल को बढ़ाना (50 लाख – 1 करोड़ तक के अनुदान के लिए सभी विषयों के लिए लागू) और घटक 3- निधि उच्च प्रभाव अनुसंधान परियोजनाएं (एक एचईआई के लिए 1 करोड़ तक और बहु-संस्थागत नेटवर्क के लिए 5 करोड़ तक का अनुदान)।
डेटाबेस: नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के पास 608 से अधिक जिलों के 3 लाख से अधिक तकनीकी विचारों का एक डेटाबेस है।
यूजीसी के बारे में:
♦ स्थापित: 1956
♦ मुख्यालय: नई दिल्ली
जल संरक्षण के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा जल शक्ति अभियान शुरू किया गया
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, ने नई दिल्ली में जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए एक अभियान ‘जल शक्ति अभियान’ (जेएसए) की शुरुआत की। यह 256 जल तनाव वाले जिलों और 1,592 जल तनाव वाले ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
प्रमुख बिंदु:
i. अभियान दो चरणों में शुरू किया गया, पहला चरण 1 जुलाई, 2019 और 15 सितंबर, 2019 के बीच, सभी भाग लेने वाले राज्यों के लिए होगा और दूसरे चरण के लिए, 1 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2019 तक, मानसून की वापसी वाले राज्यों के लिए होगा।
ii. अभियान के तहत 5 प्रमुख हस्तक्षेप क्षेत्रों में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, पारंपरिक और अन्य जल निकायों का नवीकरण, पुन: उपयोग, बोरवेल पुनर्भरण संरचनाएं, वाटरशेड विकास और गहन वनीकरण शामिल हैं।
iii.जेएसए के साथ विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर संचार अभियान की योजना भी बनाई गई थी।
जल शक्ति मंत्रालय के बारे में:
♦ स्थापित: 31 मई 2019
♦ मुख्यालय: नई दिल्ली
पीएम ने भारतीय कृषि के परिवर्तन के लिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फड़नवीस की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि को बदलने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की एक उच्च स्तरीय 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। यह नीतिगत उपायों का सुझाव देगी, निवेश को आकर्षित करेगा और खाद्य प्रसंस्करण में वृद्धि करेगी। समिति को नीति (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग द्वारा सेवित किया जाएगा।
प्रमुख बिंदु:
i. सदस्य: एच.डी.कुमारस्वामी, मुख्यमंत्री, कर्नाटक, मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री, हरियाणा, पेमा खांडू, मुख्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश, विजय रूपानी, मुख्यमंत्री, गुजरात, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, कमलनाथ, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश, केंद्रीय कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद।
ii. समय-सीमा: यह दो महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
iii. संदर्भ की शर्तें (टीओआर): समिति कृषि उपज और पशुधन, अनुबंध खेती और सेवा (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2018, कृषि उत्पादन और पशुधन विपणन (सुधार और सुविधा) अधिनियम, 2017, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में परिवर्तन, ई-एनएएम (राष्ट्रीय कृषि बाजार), जीआरएएम (ग्रामीण कृषि बाजार) और अन्य प्रासंगिक केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ बाजार सुधारों को जोड़ने के लिए तंत्र जैसे सुधारों को अपनाने और समयबद्ध कार्यान्वयन के तौर तरीकों पर सुझाव देगी।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बारे में:
♦ स्थापित: 1947
♦ मुख्यालय: नई दिल्ली
नासा के टीईएसएस स्पेस टेलीस्कोप ने एल- 98-59 बी नामक इसके सबसे छोटे ग्रह की खोज की
संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) अंतरिक्ष एजेंसी, नासा (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट (टीईएसएस) ने एल- 98-59 बी नामक एक नए ग्रह की खोज की है। यह पृथ्वी के आकार का लगभग 80 प्रतिशत है। यह एल- 98-59 तारे की परिक्रमा करता है, जो सूर्य के लगभग एक-तिहाई द्रव्यमान का है और लगभग 35 प्रकाश-वर्ष दूर है। एल 98-59 बी नामक ग्रह टीईएसएस द्वारा आज तक खोजे गए सबसे छोटे ग्रह को चिह्नित करता है।
प्रमुख बिंदु:
i. एल 98-59 की परिक्रमा करते हुए दो अन्य एक्सोप्लैनेट की भी खोज की गई जिन्हें एल 98-59 सी और एल 98-59 डी नाम दिया गया है।
ii. यह खोज द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में प्रकाशित हुई थी।
iii. टीईएसएस: यह एक अंतरिक्ष दूरबीन है जिसकी लागत नासा के खोजकर्ताओं कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 200 मिलियन डॉलर है। यह अपने पूर्ववर्ती केपलर मिशन द्वारा कवर क्षेत्र की तुलना में 400 गुना बड़े क्षेत्र में पारगमन विधि का उपयोग करके एक्सोप्लैनेट की खोज करता है।
नासा जीवन की उत्पत्ति और चिन्हों की तलाश के लिए टाइटन पर ‘ड्रैगनफ्लाई’ ड्रोन मिशन भेजेगा
अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) ने जीवन के संकेतों की खोज के लिए शनि के चंद्रमा टाइटन पर एक फ्लाइंग मल्टी रोवर वाहन, ‘ड्रैगनफ्लाई’ को भेजने की योजना बनाई है।
प्रमुख बिंदु:
i. इसे 2026 में लॉन्च किया जाएगा और 2034 में शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार किया जाएगा। मिशन का परिव्यय 850 मिलियन डॉलर था।
ii. यह नासा के न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें प्लूटो जांच न्यू होराइजन्स, बृहस्पति जांच जूनो और ओएसआईआरआईएस-रेक्स क्षुद्रग्रह मिशन शामिल हैं।
iii. मिशन: इसे नमूनों को इकट्ठा करने, टाइटन के आसपास की साइटों की जांच करने और टाइटन और पृथ्वी दोनों पर प्री बायोटिक रासायनिक प्रक्रियाओं की समानता की तलाश के उद्देश्य से लॉन्च किया जाएगा।
iv. ड्रैगन फ्लाई: यह पहली बार होगा जब नासा मल्टी-रोटर वाहन उड़ाएगा, जिसमें आठ रोटर हैं और दूसरे ग्रह पर विज्ञान के लिए एक बड़े ड्रोन की तरह उड़ते हैं।
v. टाइटन: यह शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है और बृहस्पति के चंद्रमा गेनीमेड के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है।
खगोलविदों ने फास्ट रेडियो बर्स्ट के स्रोत की खोज की
पहली बार, शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने एफआरबी 180924 के स्रोत की खोज की है, जो कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा की एक रहस्यमय शक्तिशाली पल्स है जिसे फास्ट रेडियो बर्स्ट (एफआरबी) के रूप में जाना जाता है, जो केवल एक सेकंड के एक अंश तक चली। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर (एएसकेएपी) रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके खोज की गई है।
प्रमुख बिंदु:
i. ऐसा कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति पृथ्वी से 3.6 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर मिल्की वे के आकार की आकाशगंगा के बाहरी इलाके में हुई थी।
ii. पहला एफआरबी (एफआरबी 121102) 2007 में खोजा गया था और अब तक 80 से अधिक का पता लगाया जा चुका है।
iii. एएएएस जर्नल साइंस में निष्कर्ष प्रकाशित किए गए। अध्ययन के प्रमुख लेखक कीथ बैनिस्टर थे।
नई दिल्ली में स्मृति ईरानी द्वारा डॉ.कृष्णा सक्सेना की पुस्तक ‘व्हिसपर्स ऑफ टाइम’ लॉन्च की गई
कपड़ा और महिला और बाल विकास मंत्री, स्मृति ज़ुबिन ईरानी ने नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में डॉ.कृष्णा सक्सेना (91) द्वारा लिखित नई पुस्तक ‘व्हिसपर्स ऑफ़ टाइम’ को जारी किया।
i. पुस्तक का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन ने किया था।
ii. यह सक्सेना की नौवीं पुस्तक है, और यह नब्बे साल के उनके लंबे जीवन में उनके अनुभवों और टिप्पणियों के बारे में बात करती है।
iii. सक्सेना, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश से 1955 में अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी डिग्री करने वाली पहली महिला छात्र है।
एईएस और जेई को मिटाने के लिए यूपी द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान
उत्तर प्रदेश सरकार ने घातक एक्यूट इन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) और जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई) बीमारी को मिटाने के लिए ‘दस्तक अभियान’ शुरू किया। यह एक व्यापक सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (एसबीसीसी) रणनीति का हिस्सा है जिसे यूपी सरकार ने अपनाया है।
i. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग नियंत्रण के दूसरे चरण का और दस्तक अभियान का उद्घाटन किया जो 1 से 31 जुलाई 2019 तक चलेगा।
ii. इसके तहत, अभियान टीम राज्य के 75 जिलों के प्रत्येक गांव में घर-घर जाकर संचारी रोगों के साथ-साथ जेई और एईएस के बारे में जागरूकता पैदा करेंगी।
iii.राज्य के विभाग जैसे स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा मिलकर रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे।
iv. 2018 में, यूपी सरकार ने इन्सेफेलाइटिस और अन्य वेक्टर जनित रोगों को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के सहयोग से ‘दस्तक’ अभियान शुरू किया था।
सर्वजनिक खरीद नीति
समुचित कानून का अभाव
- कोर्ट के समक्ष निविदाओं के संदर्भ में रिट दायर होने का कारण इस संदर्भ में अपर्याप्त कानूनों समेत एक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद कानून का नहीं होना हैं। भारत को सार्वजनिक खरीद नीति के लिए अभी संसदीय कानून को बनाना शेष है।
- सरकार के द्वारा लगभग सकल घरेलू उत्पाद के 30% के बराबर खरीद की जाती है। राजकोषीय रूप से इतने महत्वपूर्ण होने के बावजूद अभी तक इसके लिए कोई व्यापक कानून को अपनाया नहीं गया है। भारत में सार्वजनिक खरीद की नीति मात्र नियमों,दिशानिर्देशों और नियमों के एक चक्रव्यूह में सिमटकर रही गयी है।
- अतीत में सार्वजनिक खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों ने निर्वाचित सरकारों को सत्ता से बेदखल कर दिया है।
- वर्तमान में चल रही सभी प्रक्रियाएं में पारदर्शिता एवं कुशलता का अभाव है। ऐसे परिदृश्य में सार्वजनिक खरीद को विनियमित करने एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक यथोचित संसदीय कानून की आवश्यकता है।
- सरकार ने इस क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने हेतु 2012 में लोकसभा में सार्वजनिक खरीद विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसका उद्देश्य ” सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता,जवाबदेही और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना था”। दुर्भाग्य से यह विधेयक यह संसद द्वारा पारित नहीं किया गया।
- 2015 में तात्कालिक सरकार के द्वारा सार्वजनिक खरीद विधेयक 2015 प्रस्तुत किया गया जिसमें 2012 के प्रस्तावित विधेयक के सुधारों को भी शामिल किया गया था। परंतु यह भी अव्यवस्था का शिकार हो गई।
- प्रस्तुत किए गए दोनों विधेयकों में सार्वजनिक खरीद की शिकायतों के संदर्भ में मजबूत आंतरिक मशीनरी का प्रावधान किया गया था किंतु इन विधेयकों का कार्यान्वयन नहीं हो सका। ऐसी पृष्ठभूमि में सार्वजनिक निविदा के निर्णय को अदालतों में चुनौती देना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है।
- सार्वजनिक खरीद नीति के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान भी अपर्याप्त है। अनुच्छेद 282 सार्वजनिक व्यय में वित्तीय स्वायत्तता का प्रावधान तो करती है लेकिन सार्वजनिक खरीद के सिद्धांतों, नीतियों, प्रक्रियाओं या शिकायत निवारण के संदर्भ में कोई दिशानिर्देश प्रदान नहीं करती।
राज्यों में समुचित कानून का अभाव
- राज्य के सार्वजनिक खरीद को विनियमित करने एवं विवादों के लिए समाधान तंत्र की स्थिति राज्यों में भी अच्छी नहीं है।
- राज्य के अधिनियम के द्वारा मात्र पांच राज्यों में सार्वजनिक खरीद की जाती है: तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और असम। इन अधिनियमों में शिकायत निवारण तंत्र ना ही स्वतंत्र है एवं ना ही प्रभावी।
- मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण को प्रभावशाली रूप में कार्य करने हेतु कुछ प्रभावपूर्ण वैकल्पिक उपायों के दिशा निर्देश दिए गए। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 226 में वर्णित ‘प्रभावकारी’ शब्द पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बल प्रदान किया गया था। किंतु दुर्भाग्य से न्यायाधिकरण में इन वैकल्पिक उपायों का अभाव है।
- निविदाओं को अदालतों में चुनौती दिए जाने पर अदालतों ने न्यायिक समीक्षा के द्वारा केस-दर-केस कड़े प्रतिबंध लगाए गए, जिससे हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत ही सीमित हो गई है। खरीद अधिकारी को न्यायिक सिद्धांतों द्वारा सशक्त किया जाता है जिसमें कम कानून के साथ जवाबदेही भी कम होती है।
- अदालतों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावकारी तंत्र की अनुपस्थिति से सार्वजनिक खरीद से जुड़े नकारात्मक पहलुओं को प्रोत्साहित करेंगे।
- इस तरह के निराशाजनक कानूनी परिदृश्य में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सार्वजनिक खरीद निविदा के निर्णय को अक्सर संवैधानिक अदालतों में चुनौती दी जाती है। जब तक कोई प्रभावी विकल्प उपलब्ध नहीं करवाए जाते तब तक ऐसे मामले न्यायालयों के समक्ष आते रहेंगे।
Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY)
परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) के प्रमुख प्रोजेक्ट नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एनएमएसए) का एक विस्तृत घटक है ।
कार्यान्वयन :
- पीकेवीवाई के तहत जैविक कृषि को क्लस्टर दृष्टिकोण और पीजीएस प्रमाणीकरण द्वारा जैविक गांव को अपनाने के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है ।
- पचास या अधिक किसान इस योजना के तहत जैविक खेती करने के लिए 50 एकड़ जमीन वाले क्लस्टर का निर्माण करेंगे ।
- उत्पादन कीटनाशक अवशेष मुक्त होगा और उपभोक्ता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में योगदान देगा।
जैविक खेती और इसका महत्व:
जैविक खेती में रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग शामिल नहीं है और इस प्रकार विभिन्न जटिल पारिस्थितिक तंत्रों के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। साथ ही यह मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करता है जो वहां पैदा होने वाली फसलों के मानकों को और बेहतर बनाता है। दीर्घावधि में, जैविक खेती से कृषि, जैव-विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का निर्वाह होता है। यह मृदा स्वास्थ्य के निर्माण में भी मदद करेगा जिसके परिणामस्वरूप फसल का उत्पादन लगातार बढ़ेगा।
गैर – संचारी रोग(Non-communicable dieases)
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की रिपोर्ट के अनुसार, “ भारत राष्ट्र के राज्यों का स्वास्थ्य “(India: Health of the Nation’s States) शीर्षक, गैर-संचारी रोगों का योगदान (NCDs) देश में कुल मृत्यु का आंकड़ा 2016 में 61.8% था, जबकि 1990 में 37.9% था ।
- महामारी संक्रमण के कारण केरल, गोवा और तमिलनाडु राज्यों में कम से कम मौतों को कम्यूनिकेबल, मातृ, नवजात और पोषण संबंधी बीमारियों के लिए दर्ज किया जाता है, जिससे कुल मौतों में एनसीडी का हिस्सा बढ़ जाता है।
- एनसीडी के जोखिम कारकों में उम्र बढ़ने, अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक गतिविधि की कमी, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त शर्करा, उच्च कोलेस्ट्रॉल और अधिक वजन शामिल हैं।
एनसीडी क्या हैं?
गैर-संचारी रोग (एनसीडी), जिसे पुरानी बीमारियां भी कहा जाता है , लंबी अवधि की होती हैं और ये आनुवांशिक, शारीरिक, पर्यावरणीय और व्यवहार कारकों के संयोजन का परिणाम होती हैं।
एनसीडी के मुख्य प्रकार हृदय रोग (जैसे दिल के दौरे और स्ट्रोक), कैंसर, पुरानी सांस की बीमारियां (जैसे पुरानी प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग और अस्थमा) और मधुमेह हैं।
एनसीडी के सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या हैं?
- NCDs ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा की दिशा में प्रगति की बात कही है , जिसमें 2030 तक एनसीडी से समय से पहले होने वाली मौतों को एक तिहाई से कम करने का लक्ष्य शामिल है ।
- गरीबी एनसीडी के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है । एनसीडी में तेजी से वृद्धि की भविष्यवाणी कम आय वाले देशों में गरीबी में कमी की पहल को लागू करने के लिए की गई है, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी घरेलू लागतों को बढ़ाकर। खासकर कमजोर और सामाजिक रूप से वंचित लोग उच्च सामाजिक पदों के लोगों की तुलना में जल्दी बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं, क्योंकि वे हानिकारक उत्पादों, जैसे तम्बाकू, या अस्वास्थ्यकर आहार प्रथाओं के संपर्क में होने का अधिक जोखिम रखते हैं, और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच रखते हैं।
- कम-संसाधन सेटिंग में, एनसीडी के लिए स्वास्थ्य देखभाल की लागत घरेलू संसाधनों को जल्दी से खत्म कर देती है । NCDs की अत्यधिक लागत, जिसमें अक्सर लंबा और महंगा उपचार और ब्रेडविनर्स का नुकसान शामिल है, लाखों लोगों को सालाना गरीबी और स्टिफल विकास में मजबूर करता है।
अमेरिकी सीनेट ने अपने नाटो सहयोगियों के साथ भारत को एक सममूल्य पर लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
अमेरिकी सीनेट ने एक विधायी प्रावधान पारित किया है जो भारत को वाशिंगटन के उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सहयोगियों और इजरायल और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिएबराबर लाता है।
इसमें क्या शामिल है?
विधायी प्रावधान हिंद महासागर में मानवीय सहायता, आतंकवाद निरोध, समुद्री डकैती और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों में अमेरिका-भारत रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए प्रदान करता है ।
महत्व :
अमेरिका ने 2016 में भारत को ” प्रमुख रक्षा साझेदार ” के रूप में मान्यता दी है। यह भारत को अमेरिका के निकटतम सहयोगियों और सहयोगियों के साथ अमेरिका से अधिक उन्नत और संवेदनशील तकनीकों को खरीदने की अनुमति देता है , और इस क्षेत्र में स्थायी सहयोग सुनिश्चित करता है। एनडीएए का पारित होना अधिक विस्तार से स्पष्ट करता है कि वास्तव में निकट रक्षा सहयोग का क्या मतलब है और क्या होता है।
पहला एनडीएए 1961 में पारित किया गया था।
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के बारे में:
- यह एक अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन है ।
- 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षरित संधि ।
- मुख्यालय – ब्रुसेल्स, बेल्जियम।
- मित्र देशों की कमान संचालन का मुख्यालय – मॉन्स, बेल्जियम।
महत्व : यह सामूहिक रक्षा की एक प्रणाली का गठन करता है जिसके तहत इसके स्वतंत्र सदस्य राज्य किसी भी बाहरी पार्टी के हमले के जवाब में आपसी रक्षा के लिए सहमत होते हैं ।
उद्देश्य :
- नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और सदस्यों को समस्याओं को हल करने, विश्वास बनाने और लंबे समय में संघर्ष को रोकने के लिए रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर परामर्श और सहयोग करने में सक्षम बनाता है।
- नाटो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। यदि कूटनीतिक प्रयास विफल होते हैं, तो इसके पास संकट-प्रबंधन कार्यों को करने की सैन्य शक्ति है। ये नाटो की संधि संधि के सामूहिक रक्षा खंड के तहत किए जाते हैं – वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 या संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत, अकेले या अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से।