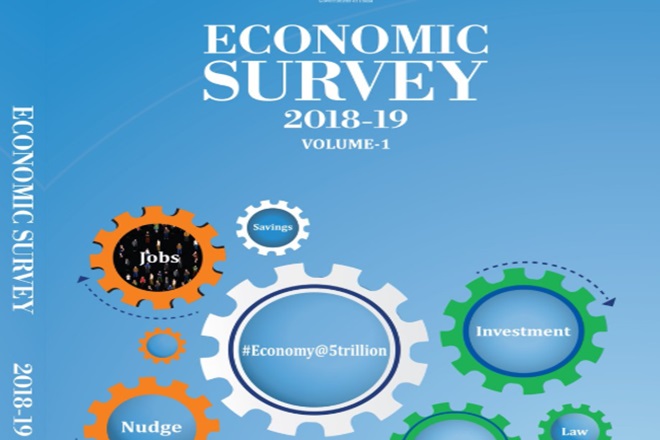Daily Current Affairs 6 July 2019
Daily current affairs:-We have Provided Daily Current Affairs for UPSC and State PCS Examinations. Current affairs is the most Important Section in the UPSC examination. To get more score in the current affairs section must Visit our Website Daily Basis.
आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19: एक अवलोकन
4 जुलाई, 2019 को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 प्रस्तुत किया। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन द्वारा तैयार किया गया था। आकाश के रंग में इसका कवर पेज था क्योंकि यह भारत के लिए उपयुक्त आर्थिक मॉडल के बारे में सोचने में एक अनपेक्षित दृष्टिकोण को अपनाता है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 की मुख्य विशेषताएं:
निजी निवेश प्रगति, रोजगार, निर्यात और मांग का मुख्य वाहक:
-आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान अमीरों को मिलने वाले लाभ के मार्ग गरीबों के लिये भी खोले गये हैं, प्रगति और वृहद अर्थव्यवस्था की स्थिरता का लाभ आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचा।
-2024-25 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए 8 प्रतिशत की सतत वास्तविक जीडीपी विकास दर की जरूरत है।
-बचत, निवेश और निर्यात को सतत विकास के लिए एक अनुकूल जनसाख्यिकी चरण द्वारा उत्प्रेरित और समर्थित ‘महत्वपूर्ण चक्र’ आवश्यक है।
-निजी निवेश – मांग, क्षमता, श्रम उत्पादकता, नई प्रौद्योगिकी, रचनात्मक खंडन और नौकरी सृजन का मुख्य वाहक है।
-सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था को एक पुण्य या दुष्चक्र के रूप में देखता है, और संतुलन में कभी नहीं।
व्यवहार अर्थशास्त्र:
-वास्तविक लोगों द्वारा निर्णय शास्त्रीय अर्थशास्त्र और व्यावहारिक अर्थशास्त्र में अव्यावहारिक रोबोटों से विचलित होते हैं, जो वांछनीय व्यवहार के प्रति लोगों को उकसाते हैं।
-व्यवहारिक अर्थशास्त्र से निम्नलिखित अंतर्दृष्टि का उपयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए एक आकांक्षात्मक एजेंडा बनाने में मदद करेगा:
-‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ से ‘बदलाव’ तक (बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी)।
-‘स्वच्छ भारत’ से ‘सुंदर भारत’ तक।
– एलपीजी सब्सिडी के लिए ‘गिव ईट उप’ से ‘थिंक अबाउट सब्सिडी’।
-‘कर चोरी’ से ‘कर अनुपालन’ तक।
एमएसएमई विकास के लिए नये सिरे से नीतियां बनाना:
-सर्वेक्षण में एमएसएमई को अधिक लाभ अर्जित करने, रोजगार जुटाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विकास योग बनाने पर ध्यान दिया गया है।
-दस साल पुरानी होने के बावजूद सौ कामगारों से कम कार्य बल वाली बौनी यानी छोटी फर्मो की संख्या विनिर्माण में लगी सभी संगठित फर्मों में पचास प्रतिशत से अधिक है। छोटी फर्मो का रोजगार में केवल 14 प्रतिशत और उत्पादकता में आठ प्रतिशत योगदान है।
-सौ से अधिक कर्मचारियों वाली बड़ी फर्मो का संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी 15 प्रतिशत होने के बावजूद रोजगार में 75 प्रतिशत और उत्पादकता में 90 प्रतिशत योगदान है।
-सर्वेक्षण में होटल, खानपान, परिवहन, रीयल इस्टेट, मनोरंजन तथा रोजगार सृजन के लिए अधिक ध्यान देते हुए पर्यटन जैसे सेवा क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
निचली अदालतों की क्षमता बढ़ाने के लिए मत्स्यन्याय को समाप्त करना:
-समझौता लागू करने और निपटान समाधान डेरी से भारत में व्यापार को सरल बनाने और उच्च जीडीपी प्रगति में एक सबसे बड़ी बाधा है। लगभग 87.5 प्रतिशत मामले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं।
-शत-प्रतिशत निपटान दर निचली अदालतों में 2279 तथा उच्च न्यायालयों में 93 खाली पदों को भरने से ही प्राप्त की जा सकती हैं।
-उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है। निचली अदालतों में 25 प्रतिशत उच्च न्यायालयों में चार प्रतिशत और उच्च न्यायालय में 18 प्रतिशत उत्पादकता सुधार से बैकलॉग समाप्त किया जा सकता है।
निवेश पर आर्थिक नीति की अनिश्चितता का प्रभाव:
अनिश्चितता ने भारत में लगभग पाँच तिमाहियों के लिए निवेश की वृद्धि को कम कर दिया।
सर्वेक्षण ने निम्नलिखित द्वारा आर्थिक नीति की अनिश्चितता में कमी करने का प्रस्ताव दिया:
-सर्वेक्षण ने आर्थिक नीति की अनिश्चितता में कमी का प्रस्ताव दिया
-सरकारी विभागों में प्रक्रियाओं का गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणन
2040 में भारत की जनसांख्यिकी, सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि:
-अगले दो दशकों में जनसंख्या की वृद्धि दर में तेजी से कमी आने की संभावनाएं है।
-2021 तक राष्ट्रीय कुल गर्भधारण दर, प्रतिस्थापन दर से कम रहने की संभावना है।
-2021-31 के दौरान कामकाजी आयु वाली आबादी में मोटे तौर पर 9.7 मिलियन प्रति वर्ष और 2031-41 के दौरान 4.2 मिलियन प्रति वर्ष वृद्धि होगी।
-अगले दो दशकों में प्रारंभिक स्कूल में जाने वाले बच्चों (5 से 14 साल आयु वर्ग) में काफी कमी आएगी। राज्यों को नये विद्यालयों का निर्माण करने के स्थान पर स्कूलों का एकीकरण/विलय करके उन्हें व्यवहार्य बनाने की आवश्यकता है।
-नीति निर्माताओं को स्वास्थ्यहुए सेवाओं में निवेश करते हुए और चरणबद्ध रूप से सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करते हुए वृद्धावस्था के लिए तैयार रहने की जरूरत है।
स्वच्छ भारत मिशन का विश्लेषण:
-स्वच्छ भारत मिशन का विश्लेषण
-जिन लोगों की शौचालयों तक पहुंच है, उनमें से 96.6 प्रतिशत ग्रामीण भारत में उनका उपयोग कर रहे है।
-30 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 100 प्रतिशत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) की कवरेज।
-परिवारों के लिए घरेलू शौचालय से वित्तीय बचत, वित्तीय लागत से औसतन 1.7 गुना और गरीब परिवारों के लिए 2.4 गुना बढ़ गई है।
-दीर्घकालिक सतत सुधारों के लिए पर्यावरणीय और जल प्रबंधन संबंधी मामलों को एसबीएम में शामिल किये जाने की जरूरत है।
किफायती विश्वसनीय और सतत ऊर्जा के माध्यम से समावेशी वृद्धि सक्षम बनाना:
-भारत को 2010 के मूल्यों पर अपने वास्तविक प्रति व्यक्ति जीडीपी में 5,000 डॉलर तक की वृद्धि करने और उच्च मध्य आय वर्ग में दाखिल होने के लिए अपनी प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में 2.5 गुना वृद्धि किये जाने की जरूरत है।
-0.8 मानव विकास सूचकांक अंक प्राप्त करने के लिए भारत को प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में चार गुना वृद्धि किये जाने की जरूरत है।
-पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अब भारत चौथे, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पांचवें और नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापित क्षमता के क्षेत्र में पांचवें स्थान पर है। संचयी नवीकरणीय बिजली स्थापित क्षमता (25 मेगावाट से अधिक हाइड्रो को छोड़कर) 31 मार्च, 2014 को 35 गीगावॉट से 31 मार्च, 2019 को 78 गीगावॉट होकर दोगुना से अधिक हो गई। लक्ष्य वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट की नवीकरणीय आधारित बिजली की स्थापित क्षमता हासिल करना है।
-संचयी नवीकरणीय बिजली स्थापित क्षमता (25 मेगावाट से अधिक हाइड्रो को छोड़कर) 31 मार्च, 2014 को 35 गीगावॉट से 31 मार्च, 2019 को 78 गीगावॉट होकर दोगुना से अधिक हो गई। लक्ष्य वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट की नवीकरणीय आधारित बिजली की स्थापित क्षमता हासिल करना है।
-देश में कुल विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय विद्युत का अंश (पनबिजली के 25 मेगावाट से अधिक को छोड़कर) 2014-15 के 6 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 10 प्रतिशत हो गया।
-60 प्रतिशत अंश के साथ तापीय विद्युत अभी भी प्रमुख भूमिका निभाती है।
-भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बाजार हिस्सेदारी मात्र 0.06 प्रतिशत है, जबकि चीन में यह 2 प्रतिशत और नॉर्वे में 39 प्रतिशत है।
मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम):
-सर्वेक्षण में कहा गया है कि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के जरिये मनरेगा योजना को सुचारू बनाये जाने से उसकी दक्षता में वृद्धि हुई है।
-नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (एनईएफएमएस) और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) को अपनाने के साथ मनरेगा में मजदूरी के भुगतान में देरी में महत्वपूर्ण कमी देखी गई।
-मनरेगा योजना के अंतर्गत विशेषकर संकटग्रस्त जिलों में कार्य की मांग और आपूर्ति बढ़ी है।
-आर्थिक संकट के दौरान मनरेगा योजना के अंतर्गत समाज के असहाय वर्ग अर्थात् महिलाएं, अजा और अजजा कार्य बल में वृद्धि हुई है।
न्यूनतम वेतन प्रणाली पुनर्निर्धारण:
-सर्वेक्षण में कामगारों की रक्षा और गरीबी के उन्मूलन के लिए बेहतर तरीके से निर्मित न्यूनतम वेतन प्रणाली की पेशकश की है। भारत में प्रत्येक तीन में से एक दिहाड़ी मजदूर न्यूनतम वेतन कानून के द्वारा सुरक्षित नहीं है।
-सर्वेक्षण न्यूनतम वेतन को तर्कसंगत बनाये जाने का समर्थन करता है, जैसा कि वेतन संबंधी संहिता विधेयक के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है।
-केन्द्र सरकार द्वारा पांच भौगोलिक क्षेत्रों में पृथक ‘नेशनल फ्लोर मिनिमम वेज’ अधिसूचित किया जाना चाहिए।
-राज्यों द्वारा या तो कौशल पर या भौगोलिक क्षेत्र पर या दोनों आधारों पर न्यूनतम वेतन ‘फ्लोर वेज’ से कम स्तरों पर निर्धारित नहीं होना चाहिए।
-सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए न्यूनतम वेतन प्रणाली को सरल और कार्यान्वयन योग्य बनाने का प्रस्ताव रखता है।
-सर्वेक्षण द्वारा न्यूनतम वेतन के बारे में नियमित अधिसूचनाओं के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ‘नेशनल लेवल डैशबोर्ड’का प्रस्ताव किया गया है।
अर्थव्यवस्था की स्थिति:
-2018-19 में भारत अब भी तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
–जीडीपी की वृद्धि दर वर्ष 2017-18 में 7.2 प्रतिशत की जगह वर्ष 2018-19 में 6.8 प्रतिशत हुई।
-2018-19 में मुद्रास्फीति की दर 3.4 प्रतिशत तक सीमित रही।
-सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में फंसे हुए कर्ज दिसम्बर, 2018 के अंत में घटकर 10.1 प्रतिशत रह गये, जोकि मार्च 2018 में 11.5 प्रतिशत थे।
-स्थिर निवेश में वृद्धि दर 2016-17 में 8.3 प्रतिशत से बढ़कर अगले साल 9.3 प्रतिशत और उससे अगले साल 2018-19 में 10.0 प्रतिशत हो गई।
-चालू खाता घाटा जीडीपी के 2.1 प्रतिशत पर समायोजित करने योग्य है।
-केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2017-18 में जीडीपी के 3.5 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 3.4 प्रतिशत रह गया।
-भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जून 2019 में 422.2 बिलियन डॉलर रखा गया है।
-सर्वेक्षण में सकल घरेलू उत्पाद का 2019-20 में 7% बढ़ने का अनुमान है।
राजकोषीय घटनाक्रम:
-जीडीपी के 3.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे और 44.5 प्रतिशत (अनंतिम) के ऋण-जीडीपी अनुपात के साथ वित्त वर्ष 2018-19 का समापन
-जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार, वर्ष 2017-18 के मुकाबले वित्त वर्ष 2018-19 के अनंतिम अनुमान में केन्द्र सरकार के कुल परिव्यय में 0.3 प्रतिशत की कमी, राजस्व व्यय में 0.4 प्रतिशत की कमी और पूंजीगत व्यय में 0.1 प्रतिशत की वृद्धि
-संशोधित राजकोषीय सुदृढ़ीकरण मार्ग के तहत वित्त वर्ष 2020-21 तक जीडीपी के 3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे और वर्ष 2024-25 तक जीडीपी के 40 प्रतिशत केन्द्र सरकार ऋण को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है।
-वित्त वर्ष 2018-19 में सामान्य राजकोषीय घाटा पर 5.8% आंका गया था।
मुद्रा प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता:
-एनपीए अनुपात में गिरावट के साथ बैंकिंग प्रणाली में सुधार हुआ और ऋण वृद्धि में तेजी आई।
-दिवाला और दिवालियापन संहिता से बड़ी मात्रा में फंसे कर्जों का समाधान हुआ और व्यापार संस्कृति बेहतर हुई।
-31 मार्च, 2019 तक सीआईआरपी (कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस) के तहत 1,73,359 करोड़ रुपये के दावे वाले 94 मामलों का समाधान हुआ।
-28 फरवरी, 2019 तक 2.84 लाख करोड़ रुपये के 6079 मामले वापस ले लिये गए।
-आरबीआई की रिपोर्ट की अनुसार फंसे कर्ज वाले खातों से बैंकों ने 50,000 करोड़ रुपये प्राप्त किए।
-अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपयों को गैर-मानक से मानक परिसंपत्तियों में अपग्रेड किया गया।
-बैंचमार्क नीति दर पहले 50 बीपीएस बढ़ाई गई और फिर पिछले वर्ष बाद में 75 बीपीएस घटा दी गई।
-सितंबर, 2018 से तरलता स्थिति कमजोर रही और सरकारी बॉन्डों पर इसका असर दिखा।
-एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) क्षेत्र में दबाव और पूंजी बाजार से प्राप्त किए जाने वाले इक्विटी वित्त उपलब्धता में कमी के कारण वित्तीय प्रवाह संकुचित रहा।
-2018-19 के दौरान सार्वजनिक इक्विटी जारी करने के माध्यम से पूंजी निर्माण में 81 प्रतिशत की कमी आई।
-एनबीएफसी के ऋण विकास दर में मार्च, 2018 के 30 प्रतिशत की तुलना में मार्च, 2019 में 9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
मूल्य और महंगाई दर:
-सीपीआईसी (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – संयुक्त) पर आधारित महंगाई दर में लगातार 5वें वर्ष गिरावट दर्ज की गई। पिछले 2 वर्षों से यह 4 प्रतिशत से कम रही है।
-उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) आधारित खाद्य मुद्रा स्फ्रीति में भी लगातार 5वें वर्ष गिरावट दर्ज की गई और ये पिछले 2वर्षों के दौरान 2 प्रतिशत से भी कम रही है।
-2018-19 के दौरान सीपीआई-सी आधारित महंगाई दर के मुख्य कारक हैं आवास, ईंधन व अन्य। मुख्य महंगाई दर के निर्धारण में सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ा है।
-2017-18 की तुलना में 2018-19 के दौरान सीपीआई ग्रामीण महंगाई दर में कमी आई है।
सतत विकास और जलवायु परिवर्तन:
-भारत का एसडीजी सूचकांक अंक राज्यों के लिए 42 से 69 के बीच और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 57 से 68 के बीच है।
-राज्यों में 69 अंकों के साथ केरल और हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है। केन्द्रशासित प्रदेशों में चंडीगढ़ और पुद्दुचेरी क्रमशः 68 और 65 अंकों के साथ सबसे आगे हैं।
-नमामि गंगे मिशन को 20,000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) 6 प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया था।
-वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए एक अखिल भारतीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) को 2019 में एक पूर्ण भारत समयबद्ध रणनीति के रूप में शुरू किया गया था।
विदेशी क्षेत्र:
-डब्ल्यूटीओ के अनुसार विश्व व्यापार का विकास 2017 के 4.6 प्रतिशत की तुलना में 2018 में कम होकर 3 प्रतिशत रह गया है।
-दिसंबर, 2018 तक भारत का विदेशी ऋण 521.1 बिलियन डॉलर था। यह मार्च, 2018 के स्तर से 1.6 प्रतिशत कम है।
-कुल देयताएं और जीडीपी का अनुपात (ऋण और गैर-ऋण घटकों के समावेश के साथ) 2015 के 45 प्रतिशत से कम होकर 2018 में 38 प्रतिशत हो गया है।
-2017-18 के दौरान भारतीय रुपये का मूल्य प्रति डॉलर 65-68 रुपये था। परन्तु अवमूल्यन के साथ भारतीय रुपये का मूल्य 2018-19 के दौरान प्रति डॉलर 70-74 रुपये हो गया।
-2018-19 में भारत के निर्यात आयात बास्केट का स्वरूप:
निर्यात (पुनर्निर्यात सहित): 23,07,663 करोड़ रुपये
आयातः 35,94,373 करोड़ रुपये
-सबसे ज्यादा निर्यात वाली वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती पत्थर, दवाएं के नुस्खे, स्वर्ण और अन्य कीमती धातु शामिल रहीं।
-सबसे ज्यादा आयात वाली वस्तुओं में कच्चा तेल, मोती, कीमती पत्थर तथा सोना शामिल रहा।
-भारत के मुख्य व्यापार साझेदारों में अमेरिका, चीन, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात और सउदी अरब शामिल रहे।
-भारत ने 2018-19 में विभिन्न देशों/देशों के समूह के साथ 28 द्विपक्षीय, बहु-पक्षीय समझौते किए।
-इन देशों को कुल 121.7 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का निर्यात किया गया, जोकि भारत के कुल निर्यात का 36.9 प्रतिशत था।
-इन देशों से कुल 266.9 अरब डॉलर मूल्य का आयात हुआ, जो भारत के कुल आयात का 52.0 प्रतिशत रहा।
कृषि और खाद्य प्रबंधन:
-सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) 2014-15 में देश के कृषि क्षेत्र ने 0.2 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि से उबरकर 2016-17 में 6.3 प्रतिशत की विकास दर हासिल की, लेकिन 2018-19 में यह घटकर 2.9 प्रतिशत पर आ गई।
-सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) 2017-18 में कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण 15.2 प्रतिशत घटा। 2016-17 में यह 15.6 प्रतिशत रहा था।
-कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 2005-06 के अवधि के 11.7 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 में बढ़कर 13.9 प्रतिशत हो गई।
-89 प्रतिशत भू-जल का इस्तेमाल सिंचाई कार्य के लिए किया गया है।
-नीतियां डेयरी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, और पशुधन पालन, मत्स्य पालन क्षेत्र में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
उद्योगों और अवसंरचना:
-विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता रिपोर्ट 2019 में भारत 2018 में दुनिया के 190 देशों में पहले की तुलना में 23 स्थान ऊपर आ कर 77वें स्थान पर पहुंचा।
-2018-19 में देश में सड़क निर्माण कार्यों में 30 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से तरीकी हुई।
-2018-19 में रेल ढुलाई और यात्री वाहन क्षमता में क्रमशः 5.33 और 0.64 की वृद्धि हुई।
-देश में 2018-19 के दौरान कुल टेलीफोन कनेक्शन 118.34 करोड़ पर पहुंच गए। जीडीपी में दूरसंचार उद्योग का योगदान 2020 तक 8.2% तक पहुंचने का अनुमान है।
-सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) बुनियादी ढाँचों को संबोधित करने के लिए आदर्श हैं।
-प्रधानमंत्री आवास योजना और सौभाग्य (प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना) योजनाओं जैसे प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से टिकाऊ और लचीली अवसंरचनाओं को खास महत्व दिया गया।
–2032 तक 10 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के आकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एक मजबूत और लचीला बुनियादी ढांचा प्रणाली की आवश्यकता है, जो पर्याप्त निजी निवेशों द्वारा समर्थित हो।
सेवा क्षेत्र:
-सेवा क्षेत्र ने 2018-19 में जीवीए की वृद्धि में आधे से अधिक योगदान दिया है।
-2017-18 में आईटी-बीपीएम उद्योग 8.4 प्रतिशत बढ़कर 167 अरब अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया।
-2018-19 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि मामूली घटकर 7.5% रह गई।
–जिन क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई वे वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं थीं।
-जिन क्षेत्रों में गिरावट देखी गई वे होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण सेवाएं थीं।
सामाजिक बुनियादी ढांचा, रोजगार और मानव विकास:
-स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च 2014-15 में 1.2% से बढ़कर 2018-19 में 1.5% हो गया।
-2018-19 में शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़कर 3% हो गया।
-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा रही है।
-शिक्षा के मात्रात्मक और गुणात्मक संकेतकों में पर्याप्त प्रगति आई, जिसमें नाम लिखवाने के सकल अनुपात, लिंग समानता सूचकांक और प्राइमरी स्कूल के स्तर पर पढ़ाई के नतीजों में सुधार दिखाई दिया।
-कर्मचारी भविष्य – निधि संस्था (ईपीएफओं) के अनुसार औपचारिक क्षेत्र में मार्च 2019 में रोजगार सृजन उच्च स्तर पर 8.15 लाख था, जबकि फरवरी 2018 में यह 4.87 लाख था।
-31 मार्च, 2019 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 1 करोड़ पक्के मकानों के लक्ष्य के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत लगभग 1.54 करोड़ घर पूरे हुए।
स्मार्ट सिटी मिशन:
सर्वेक्षण से पता चला कि स्मार्ट शहरों मिशन के तहत 100 शहरों में 2.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में:
आर्थिक सर्वेक्षण एक वार्षिक दस्तावेज है जिसे सरकार ने पिछले एक साल में आर्थिक विकास की समीक्षा करते हुए तैयार किया है।
वर्ष 2019-20 के लिए 24 लाख 57 हजार 235 करोड़ रूपये का केन्द्रीय आम बजट प्रस्तुत किया गया
देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को वर्ष 2019-20 के लिए 24 लाख 57 हजार 235 करोड़ रूपये का केन्द्रीय आम बजट प्रस्तुत किया. यह NDA सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट था. बुनियादी ढांचे का विकास, भारत को 50 खरब डालर वाली अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना, किसान कल्याण और जल सुरक्षा इस बजट की मुख्य बातें हैं.
आम बजट सरकार के वार्षिक राजस्व और व्यय तथा आगामी वर्ष के अनुमानित व्यय अनुमानों का ब्यौरा प्रस्तुत करता है. मोदी सरकार ने बजट को लेकर कई परंपराओं को बदला है. पहले फरवरी के अंतिम दिन बजट पेश होता था, जिसे बदलकर अब 1 फरवरी कर दिया गया है. लेकिन इस बार पिछली सरकार में अंतरिंम बजट पेश किया गया था इसलिए अब सरकार संसद के पहले सत्र में पूर्ण बजट पेश करने का निर्णय लिया. यही नहीं सरकार ने रेल बजट को भी खत्म करके आम बजट में शामिल कर लिया है.
2014-2019 के दौरान की उपलब्धियां
- पिछले पांच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन डॉलर की राशि जुड़ी है.
- भारत विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है. पांच वर्ष पहले यह 11वें स्थान पर था.
- क्रय शक्ति की समानता के दृष्टि से भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है.
- 2009-14 की तुलना में 2014-19 के बीच खाद्य सुरक्षा पर प्रतिवर्ष औसतन दोगुना खर्च किया गया.
- 2014 की तुलना में 2017-18 में तिगुने से भी अधिक पेटेंट जारी किये गये.
- नीति आयोग की योजाओं और समर्थन से नये इंडिया के निर्माण की प्रक्रिया जारी है.
रुपया कहाँ से आया और कहाँ गया
वित्त वर्ष 2018-19 के आम बजट के अनुसार सरकार की आमदनी और खर्च का ब्योरा प्रतिशत में इस प्रकार है:
| सरकार की आमदनी | सरकार का खर्च |
| ऋण से इतर पूंजी प्राप्तियां: 3% कर से इतर राजस्व: 9% वस्तु एवं सेवा कर (GST) : 19% केन्द्रीय उत्पाद शुल्क: 8% सीमा शुल्क: 4% आय कर: 16% निगम कर: 21% उधार और अन्य देयताएं: 20% |
ब्याज: 18% रक्षा: 9% सब्सिडी: 8% वित्त आयोग और अन्य खर्च: 7% करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा: 23% पेंशन: 5% केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं: 9% केन्द्रीय क्षेत्र की योजना: 13% अन्य खर्च: 8% |
बजट में अगले दस साल के विजन
बजट में अगले दस साल के विजन को भी प्रस्तुत किया गया है. इसके अंतर्गत मौलिक और सामाजिक अवसंरचना के विकास, डिजिटिल इंडिया, प्रदूषण मुक्त भारत, मेक इन इंडिया, जल प्रबंधन और नदियों की सफाई, अंतरिक्ष कार्यक्रम, खाद्यान आत्मनिर्भरता और निर्यात बढ़ाने, स्वस्थ समाज और जन भागीदारी के साथ टीम इंडिया भावना को विकसित करने की बात कही गई है.
5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था की परिकल्पना
2014 में जब NDA सरकार सत्ता में आई तो भारतीय अर्थव्यवस्था 18.5 खरब डॉलर की थी और पांच साल के भीतर यह 27 खरब डॉलर की हो गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 55 साल में 1 ट्रिलियन की बनी थी जबकि यही उपलब्धि पिछले 5 सालों में हासिल की गयी.
वित्त मंत्री ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान वर्ष में 30 खरब डॉलर (3 ट्रिलियन डॉलर) हो जाएगी और यह 2024-25 तक 50 खरब डॉलर (5 ट्रिलियन डॉलर) की अर्थव्यवस्था बनने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना को हासिल करने के रास्ते पर है. वित्त मंत्री ने कहा कि देश की 50 खरब डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिये बुनियादी ढांचा, डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारी निवेश और रोजगार सृजन पर जोर देने की योजना है.
2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को बिजली और रसोई गैस
बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री सीतारामन ने ग्रामीण परिवारों का जीवन बदलने वाली उज्जवला और सौभाग्य योजनाओं का जिक्र किया. उन्होंने आश्वासन दिया कि 2022 यानी भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को बिजली और रसोई गैस उपलब्ध हो जायेगी.
राजघाट में राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र
वित्तमंत्री ने कहा कि गांधीजी की 150वीं सालगिरह पूरे के अवसर पर 2 अक्तूबर 2019 को राजघाट में राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र का उद्घाटन किया जायेगा. वित्तमंत्री ने आशा व्यक्त की कि भारत इस साल गांधी जयंती तक खुले में शौच की कुप्रथा से पूरी तरह मुक्त हो जायेगा.
आयकर में बदलाव नहीं
दो करोड़ रुपये तक की व्यक्तिगत आमदनी पर आयकर में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है. दो करोड़ से पांच करोड़ रुपये की कर-योग्य आय वाले व्यक्तियों पर लगने वाले अधिभार में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. पांच करोड़ से अधिक कर योग्य आय पर अधिभार में 7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है.
आधार कार्ड से भी ITR
अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स (ITR) भर पाएंगे. यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है, जिनके पास पैन नहीं है, वे आधार के जरिए ITR दाखिल कर सकते हैं.
घर खरीदने पर 3.5 लाख छूट
अब 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी. हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है. इसके अलावा 2.5 लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी.
बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान
वर्ष 2019-20 के बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है. भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण की शुरूआत की जाएगी जिसके अंतर्गत देश भर में सड़क संपर्क का विस्तार किया जायेगा.
2022 तक हर किसी को घर देने का लक्ष्य
सरकार वर्ष 2022 तक 1.95 करोड़ पात्र गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध करायेगी. पिछले पांच साल में 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध कराये गये. इससे पहले 2015-16 में जहां ऐसे मकान बनाने में 314 दिन लगते थे, वर्ष 2017-18 में यह समय घटकर 114 दिन रह गया. वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2022 तक हर किसी को घर देने का है.
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का लक्ष्य 2019 किया गया
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने की अवधि कम कर दी गई है. इस कार्यक्रम के 2022 के बजाय 2019 में ही पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है.
किसानों के कल्याण के प्रति वचनबद्धता
किसानों के कल्याण के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराते हुए वर्ष 2019-20 के बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं. कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बांस, शहद और खादी वस्तुओं पर विशेष ध्यान देने की बात भी बजट में बताई गई है. बजट में पचास हजार शिल्पकारों को सक्षम बनाने के लिए सौ नये क्लस्टर बनाने का भी कार्यक्रम है. जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक हर घर जल कार्यक्रम के अंतर्गत सभी ग्रामीण परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है. इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रबंधन, वर्षा जल संचय, भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है.
कॉरपोरेट कर लागू होने निम्नतम सीमा 400 करोड़ रुपये
वित्तमंत्री ने कॉरपोरेट कर लागू होने की निम्नतम सीमा 250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है. अब 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स देना होगा. पहले 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स देना होता था. इसके तहत देश की 99 फीसदी कंपनी आ जाएंगी.
बीमा मध्यस्थ क्षेत्र में 100 प्रतिशत FDI
वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा मध्यस्थ क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी जायेगी. सरकार विमानन, मीडिया, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) सीमा बढ़ाने के मामले में संबंध पक्षों के साथ बातचीत के बाद फैसला करेगी. दुनियाभर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पिछले तीन साल के दौरा गिरावट आने के बावजूद भारत में 6 प्रतिशत बढ़कर 64 अरब डालर से अधिक रहा है.
केन्द्रीय आम बजट 2019-20: मुख्य तथ्य
- एनडीए सरकार ने न्यू इंडिया की शुरूआत कर दी है और दुनिया को दिखा दिया है कि रिफार्म, परफार्म और ट्रासफार्म का सिद्धांत सफल हो सकता है.
- सरकार ने बजट में बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए वन नेशन वन ग्रिड की पहल की है.
- सरकार का केंद्र बिंदु गांव, किसान और गरीब है और 2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है.
- बीमा मध्यस्थ क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी जायेगी.
- दुनियाभर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पिछले तीन साल के दौरा गिरावट आने के बावजूद भारत में 6 प्रतिशत बढ़कर 64 अरब डालर से अधिक रहा है.
- भारतमाला के दूसरे चरण में राज्यों को राज्यस्तरीय सड़कों के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
- नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड के साथ ही सरकार ने MRO का फॉर्मूला अपनाने की बात कही है. जिसमें मैन्यूफैक्चरिंग, रिपेयर और ऑपरेट का फॉर्मूला लागू किया जाएगा.
- अगले पांच सालों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तकनीक का इस्तेमाल कर कार्बन मुक्त बनाया जाएगा.
- सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण घरों तक 2022 तक 100 प्रतिशत बिजली कनेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा.
- स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, ST-ST उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा.
- अब NRI को भारत आते ही आधार कार्ड देने की सुविधा मिलेगी, साथ ही अब उन्हें 180 दिनों तक भारत में रहने की जरूरत नहीं है.
- 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा.
- अब 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने पर हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गई है.
- 5 लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी.
- अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे. यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है.
कंपनी के लाभ के बंटवारे पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने इंटरनेशनल कन्वेंशन का समर्थन किया
सरकार ने हाल ही में बेस एरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस) से निपटने के लिए ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) द्वारा डिजाइन किए गए बहुपक्षीय कर कन्वेंशन संधि को लागू करने की पुष्टि की। यह बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा कर से बचने के अवसरों को कम करने के लिए किया गया है।
प्रमुख बिंदु:
i. बीईपीएस (बहुपक्षीय उपकरण (एमएलआई)) को रोकने के लिए कन्वेंशन के उपायों को भारत ने 2017 में पेरिस में हस्ताक्षरित किया था।
ii. बीईपीएस: कंपनियों द्वारा अपने लाभ को कम या बिना-कर स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए कर नियोजन रणनीति है, जहां बहुत कम या कोई आर्थिक गतिविधि नहीं होती है, जिसके परिणामस्वरूप बहुत कम या पुरे कॉर्पोरेट कर का भुगतान नहीं किया जाता है।
iii. पृष्ठभूमि: कन्वेंशन (एमएलआई) बेस एरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस प्रोजेक्ट) से निपटने के लिए ओईसीडी / जी 20 प्रोजेक्ट के परिणामों में से एक है और यह भारत के लिए 1 अक्टूबर 2019 से लागू होगा।
iv. प्रभाव: यह संधि भारत की संधियों को संशोधित करेगी ताकि संधि के दुरुपयोग और बीईपीएस रणनीतियों के माध्यम से राजस्व हानि पर अंकुश लगाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुनाफे पर कर लगाया जा रहा है जहाँ पर लाभ कमाने वाली महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियाँ की जाती हैं और जहाँ मूल्य बनता है।
v. उपयुक्ता: एमएलआई कन्वेंशन के लिए दो या अधिक पार्टियों के बीच कर संधियों को संशोधित करने के लिए काम करेगा। यह एक एकल मौजूदा संधि में संशोधन प्रोटोकॉल के समान कार्य नहीं करेगा, जो कवर किए गए कर समझौते के लेखन में संशोधन करता है। इसके बजाय, यह मौजूदा कर संधियों के साथ लागू किया जाएगा, ताकि बीईपीएस उपायों को लागू करने के लिए उनकी उपयुक्ता को संशोधित किया जा सके।
आईसीआईसीआई बैंक ने वाणिज्यिक वाहन वित्तपोषण के लिए इंडोस्टार कैपिटल के साथ समझौता किया
आईसीआईसीआई बैंक ने नए और पुराने वाणिज्यिक वाहनों को खरीदने के लिए छोटे और मध्यम बेड़े के मालिकों के लिए वाहन वित्तपोषण के लिए इंडोस्टार कैपिटल, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के साथ करार किया।
i. इंडोस्टार टीयर- II, III, IV शहरों में ग्राहकों की उत्पत्ति करेगा जहां इसकी 322 शाखाओं का शाखा नेटवर्क है और यह सोर्सिंग, प्रलेखन, संग्रह और ऋण सर्विसिंग सहित पूरे ऋण जीवन-चक्र के माध्यम से ग्राहकों को सेवा प्रदान करेगा।
ii. आईसीआईसीआई बैंक ग्राहकों को धन मुहैया कराएगा।
iii. कोयंबटूर, सलेम, तिरुनेलवेली, कुरनूल, कालीकट, त्रिवेंद्रम, जबलपुर, भोपाल, अहमदाबाद, राजकोट, जोधपुर, अलवर, और मेरठ जैसे शहरों के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
आईसीआईसीआई बैंक के बारे में:
♦ आईसीआईसीआई का मतलब इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है।
♦ मुख्यालय: मुंबई
♦ सीईओं: संदीप बख्शी
♦ टैग लाइन: हमें हैं ना, ख्याल आपका
इंडोस्टोर कैपिटल के बारे में:
♦ स्थापित: 2009
♦ सीईओं: आर.श्रीधर
आईएईए ने पुष्टि की कि ईरान ने 2015 परमाणु समझौते की समृद्ध यूरेनियम भंडार सीमा का उल्लंघन किया है
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने पुष्टि की कि ईरान ने 2015 के परमाणु समझौते / ईरान समझौते द्वारा निर्धारित इसके समृद्ध यूरेनियम भंडार पर 300 किलोग्राम की सीमा पार कर ली थी। प्रारंभ में, ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने घोषणा की थी कि ईरान ने कम समृद्ध यूरेनियम के अपने भंडार पर निर्धारित सीमा को पार कर लिया था।
ईरान डील के बारे में:
इसे संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओंए) या ईरान परमाणु समझौते के रूप में भी जाना जाता है। इस पर वियना, ऑस्ट्रिया में 14 जुलाई, 2015 को ईरान, पी 5 + 1 के बीच हस्ताक्षर किए गए- पी 5 + 1 देश फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चीन, रूस और अमेरिका (पी 5) और जर्मनी है।
सौदे के अनुसार ईरान 300 किलोग्राम से अधिक कम समृद्ध यूरेनियम का भंडार नहीं कर सकता था और उसे कम समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन करने की अनुमति थी, जिसमें यू -235 का 3.67% सांद्रता थी, जो यूरेनियम का एक आइसोटोप था, और केवल 2031 तक एक बिजली संयंत्र को ईंधन दे सकता था।
सीसीएमबी और सीडीएफडी ने नए आनुवंशिक रोग निदान विधियों को विकसित करने के लिए एमओंयू पर हस्ताक्षर किए
हैदराबाद स्थित भारतीय जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रतिष्ठान, सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (सीसीएमबी) और सेंटर फॉर डीएनए फ़िंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स (सीडीएफडी) ने आनुवंशिक विकारों के इलाज के लिए नए नैदानिक तरीकों को सक्षम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओंयू) पर हस्ताक्षर किए।
i. उद्देश्य: मानव आनुवंशिक विकारों की समझ में सुधार के लिए जनता को कम दर पर उच्च गुणवत्ता वाले डीएनए-आधारित नैदानिक सेवाएं प्रदान करने और वैज्ञानिक अनुसंधान में संलग्न करने के उद्देश्य से एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे।
ii. रिपोर्ट: भारत में, हर साल 50 लाख से अधिक बच्चे आनुवांशिक बीमारी के साथ पैदा होते हैं।
iii. डीएनए अनुक्रमण तकनीक: यह निदान के बेहतर तरीकों को सक्षम करेगा और मानव आनुवंशिक रोग के इलाज में मदद करेगा।
सीडीएफडी के बारे में:
यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संगठन है और यह जीवन विज्ञान में अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने की सुविधा के लिए विश्व स्तर के अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है।
सीसीएमबी के बारे में:
यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के तत्वावधान में संचालित होता है। केंद्र का उद्देश्य आधुनिक जीव विज्ञान के सीमांत क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी अनुसंधान और प्रशिक्षण का संचालन करना है।
यूआईडीएआई ने दिल्ली और विजयवाड़ा में अपना पहला आधार सेवा केंद्र शुरू किया
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने पायलट आधार पर दिल्ली और विजयवाड़ा में अपने पहले ‘आधार सेवा केंद्र’(एएसके) का संचालन शुरू किया है। यूआईडीएआई की 2019 के अंत तक 53 भारतीय शहरों को कवर करते हुए 114 ऐसे केंद्र स्थापित करने की योजना है। परियोजना की अनुमानित लागत 300-400 करोड़ रुपये के बीच है। ये केंद्र पासपोर्ट सेवा केंद्रों की अवधारणा के समान हैं।
एएसके की विशेषताएं:
i. इसका स्वामित्व यूआईडीएआई के पास है।
ii. यह ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से नामांकन, अपडेशन और अन्य गतिविधियों की सुविधा प्रदान करेगा, जो लोगों को उनकी सुविधा के अनुसार स्लॉट बुक करने की अनुमति देता है।
iii. एएसके केंद्र हजारों केंद्रों के अलावा हैं जो वर्तमान में डाकघरों और बैंकों और यहां तक कि सरकारी परिसरों (समान आधार सेवाओं की पेशकश कर रहे है) द्वारा चलाए जा रहे हैं।
iv. दिल्ली केंद्र – अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन परिसर में स्थित, यह एक दिन में 1,000 नामांकन / अपडेशन अनुरोधों को संभालने की क्षमता रखता है। यह 16 वर्कस्टेशनों से सुसज्जित है और सप्ताह में 6 दिन चालू रहेगा। यह केवल मंगलवार और सार्वजनिक अवकाश पर बंद रहेगा।
v. विजयवाड़ा केंद्र – विजयवाड़ा केंद्र में क्षमता एक दिन में 500 नामांकन / अपडेशन अनुरोध को संभालने की है।
यूआईडीएआई के बारे में:
♦ सीईओं: अजय भूषण पांडे
♦ मुख्यालय: नई दिल्ली
♦ स्थापित: 28 जनवरी 2009
♦ मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
स्टेट ऑफ़ एजुकेशन इन इंडिया 2019 का शुभारंभ
द स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2019 विकलांग बच्चों को हाल ही में नई दिल्ली में यूनेस्को द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम में सरकार, नागरिक समाज, शिक्षाविदों, भागीदारों और युवाओं के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
वार्षिक रूप से प्रकाशित होने के लिए, रिपोर्ट का 2019 संस्करण यूनेस्को नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित अपनी तरह का पहला है। यह विकलांग (सी डब्ल्यू डी ) बच्चों के शिक्षा के अधिकार (आर टी ई ) के संबंध में उपलब्धियों और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।
मुख्य निष्कर्ष
- संदर्भ के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के व्यापक शोध के आधार पर, रिपोर्ट विकलांग बच्चों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत और पूरी जानकारी प्रदान करती है!
- यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं को 10 महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करती है।
- यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टी आई एस एस ) द्वारा तैयार किया गया है और यूनेस्को द्वारा कमीशन किया गया है।
- 2011 की जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए, रिपोर्ट से पता चला है कि 5-19 वर्ष की आयु के बीच भारत में 78 लाख से अधिक विकलांग बच्चे हैं।
- इन विकलांग बच्चों के 27% (उम्र 5 से 19 वर्ष के बीच) ने कभी किसी शैक्षणिक संस्थान में भाग नहीं लिया।
- लगभग 75 %, 5 वर्ष के बच्चे जिनकी कुछ निश्चित अक्षमताएं हैं, वे किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नहीं जाते हैं।
- स्कूलों में लड़कों की तुलना में विकलांग लड़कियों की संख्या कम है।
- विकलांग बच्चों का अनुपात जो स्कूल से बाहर है, राष्ट्रीय स्तर पर आउट-ऑफ-स्कूल बच्चों के समग्र अनुपातसे अधिक है। ‘
- ग्रामीण भारत के कई हिस्सों में, यदि कोई माता-पिता घर-आधारित शिक्षा को चुनते हैं, तो बच्चे को वैसी शिक्षा बिल्कुल नहीं मिल रही है जैसा कि अक्सर केवल विकलांग बच्चों के लिए कागज पर मौजूद होता है।
- अपर्याप्त आवंटन, धन जारी करने में देरी और आवंटन का उपयोग विकलांग बच्चों के लिए वित्त पोषण शिक्षा में महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं।
- दृष्टि और श्रवण से संबंधित दोष वाले केवल 20% बच्चे कभी स्कूल में नहीं थे। हालांकि, कई विकलांग या मानसिक बीमारी वाले बच्चों में, यह आंकड़ा 50% से अधिक हो गया।
सुझाव:
- शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में संशोधन करें ताकि इसे विकलांग व्यक्ति के अधिकार अधिनियम, 2016 के साथ संरेखित किया जा सके।
- विकलांग बच्चों पर डेटा को मजबूत करने की आवश्यकता है जो उनकी शिक्षा की प्रभावी योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में मदद कर सकते हैं।
- केंद्रित अभियान और बड़े पैमाने पर जागरूकता होनी चाहिए जो कक्षा में और उससे परे, विकलांग बच्चों के प्रति दृष्टिकोण में सुधार कर सके।
- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के तहत तंत्र को विभागों में विकलांग बच्चों के लिए सभी शिक्षा कार्यक्रमों के समन्वय की आवश्यकता है।
- यह उनकी शिक्षा के उद्देश्य से विसंगतियों को दूर करने और विभिन्न उपायों में तालमेल हासिल करने में मदद करेगा।
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को)
- यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करना चाहता है।
- यूनेस्को के कार्यक्रम 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा अपनाये गए एजेंडा 2030 में परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की उपलब्धि में योगदान करते हैं,।
- यह विकास और सहयोग के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में वैज्ञानिक कार्यक्रमों और नीतियों को बढ़ावा देता है।
- यूनेस्को की स्थापना 16 नवम्बर 1945 में यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में की गयी थी!
- इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित है!